नवीनतम
फीचर्ड
राजनीति
भारत
जगमगाते महानगरों के भीतर पनपती खामोश महामारी
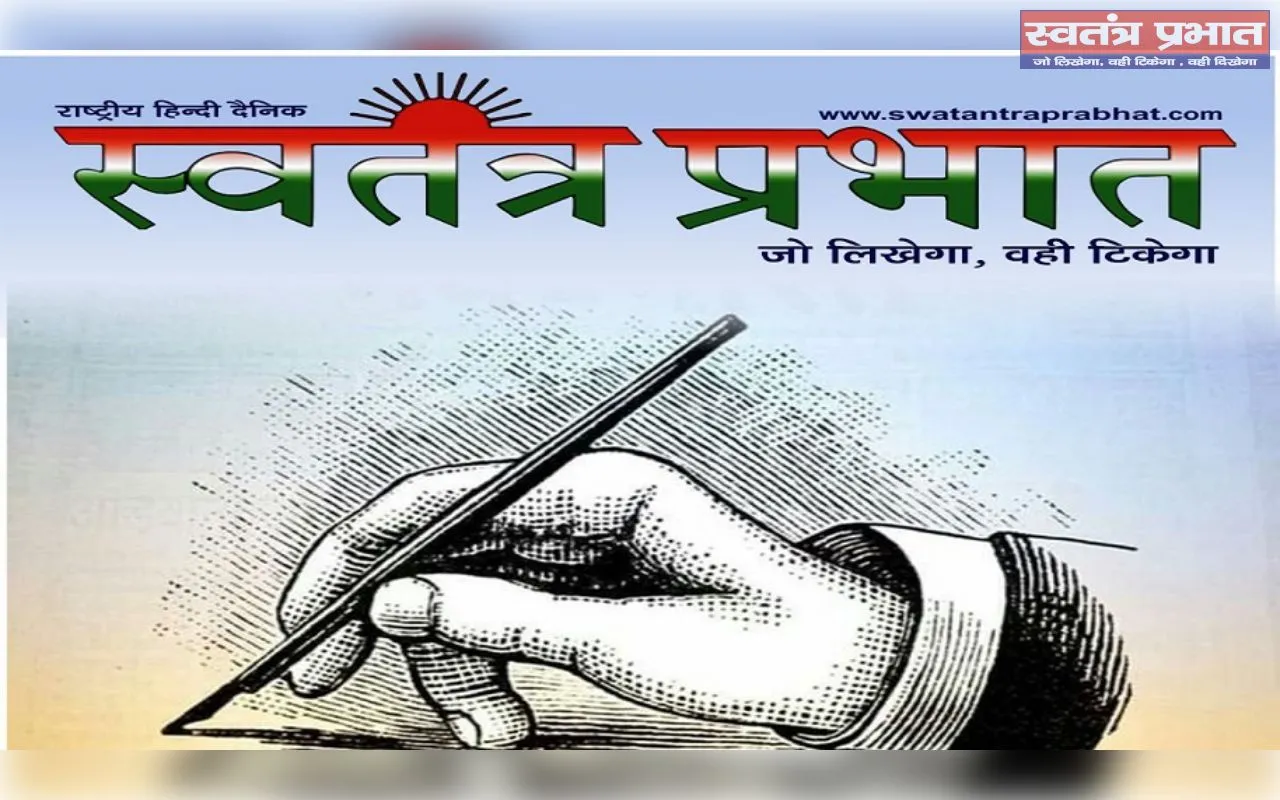
सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते लोग, भीतर से दरकते रिश्ते , महानगर: अवसरों की भूमि या संवेदनाओं का सूखा मैदान?
प्रो. आरके जैन “अरिजीत”
पहले शहरों को उम्मीदों की फैक्ट्री कहा जाता था। यहाँ रोशनी कभी बुझती नहीं, सपने थकते नहीं और भीड़ ठहरती नहीं। फिर भी इस अनवरत चहल-पहल के बीच एक गहरी खामोशी जन्म ले रही है। 1.4 अरब लोगों के देश में, जहाँ हर प्लेटफॉर्म, हर चौराहा, हर बाज़ार भीड़ से अटा है, वहीं दिलों के भीतर सूनापन फैलता जा रहा है। ऊँची इमारतों की जगमगाती खिड़कियाँ बताती हैं कि लोग मौजूद हैं, पर मौजूदगी और अपनापन अलग बातें हैं। शहरों ने हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया, मगर दिलों के बीच फासले बढ़ा दिए। यही फासला अब महामारी की तरह फैल रहा है। सर्वे बताते हैं कि 61 प्रतिशत भारतीय अकेलापन महसूस करते हैं, और युवाओं में यह दर सबसे अधिक है।
अकेलापन अब केवल निजी कमजोरी नहीं, हमारी सामाजिक बनावट की दरार है। महानगरों की दौड़ ऐसी है कि रिश्ते रास्ते में छूट जाते हैं। सुबह की सिटी बस या मेट्रो में सैकड़ों चेहरे साथ चलते हैं, पर कोई नज़र किसी पर ठहरती नहीं। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स जुड़ते हैं, पर कठिन समय में सहारा देने वाला हाथ नहीं मिलता। डिजिटल जुड़ाव ने संवाद का आभास रचा, मगर उसकी संवेदना छीन ली। इमोजी हँसते हैं, पर असली मुस्कान की गर्माहट गायब है। यह बनावटी निकटता भीतर के शून्य को और गहरा करती है—मानो भीड़ के बीच खड़ा व्यक्ति अपने ही अस्तित्व से दूर हो गया हो।
आज का शहर प्रतिस्पर्धा की प्रयोगशाला बन गया है, जहाँ हर व्यक्ति खुद को साबित करने की दौड़ में सांस ले रहा है। नौकरी की अस्थिरता, बढ़ती महँगाई, किराए का बोझ और करियर की अनिश्चितता मन पर अदृश्य दबाव बनाते हैं। आर्थिक सुरक्षा की खोज में लोग भावनात्मक सहारे से समझौता कर बैठते हैं। रिश्ते समय चाहते हैं, और समय सबसे महँगी पूँजी हो चुका है। परिवार सिमटते गए, पड़ोसी अपरिचित होते गए, दोस्तियाँ औपचारिकताओं में बदलती गईं। नतीजा यह कि इंसान सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा, पर भीतर की सीढ़ियाँ दरकती रहीं। उपलब्धियों के शोर में दिल की धीमी आवाज़ कहीं खोती चली गई।
भारत जैसे देश में, जहाँ सामूहिकता परंपरा की पहचान रही है, वहाँ भी यह बदलाव साफ दिखता है। कभी आँगन में दादी की कहानियाँ गूँजती थीं, मोहल्ले की चौपालें सजती थीं और त्योहार मिलन का बहाना बनते थे। अब त्योहार इंस्टाग्राम स्टोरी बन गए हैं, परिवार व्हाट्सऐप ग्रुप तक सिमट गया है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल जीवनशैली ने ले ली है। स्वतंत्रता तो बढ़ी है, पर सहारा कम हो गया है। आधुनिकता ने विकल्पों की भरमार दी, मगर उसी ने स्थायित्व छीन लिया। बदलते सामाजिक ढाँचे में व्यक्ति स्वायत्त तो हुआ, पर भीतर से और अधिक अकेला। यही विरोधाभास शहरों की गहरी त्रासदी बन चुका है।
रोज़गार और बेहतर भविष्य की तलाश में लाखों लोग अपने कस्बों और गाँवों से दूर आ बसे हैं। इस बदलाव ने अवसर तो दिए, पर पहचान की मिट्टी छीन ली। नए शहर में सब कुछ नया होता है—भाषा की लय, व्यवहार की शैली, जीवन की रफ्तार। व्यक्ति रोज़ाना अनुकूलन करता है, पर भीतर कहीं जड़ों की तलाश बनी रहती है। त्योहारों पर घर न पहुँच पाने की कसक, अपनों की आवाज़ से दूरी और साझा स्मृतियों का अभाव मन को अनकहा बोझ दे जाता है। नए संबंध बनते हैं, पर पुराने जैसा सहज भरोसा नहीं पनपता। यह विस्थापन बाहर से उपलब्धि लगता है, भीतर से रिक्तता का कारण बन जाता है।
मानसिक स्वास्थ्य के आँकड़े इस सच को और तीखा कर देते हैं। अवसाद, चिंता और अनिद्रा की समस्याएँ तेज़ी से फैल रही हैं। विडंबना यह कि भीड़ से भरे शहरों में भी लोग अपनी पीड़ा चुपचाप ढोते हैं; मदद माँगना अब भी कमजोरी माना जाता है। सफलता की चमक के पीछे संघर्ष की छाया दिखती नहीं। कॉर्पोरेट दफ्तरों की जगमग इमारतों में बैठे अनेक लोग भीतर से दरके होते हैं। वे पेशेवर मुस्कान ओढ़े रहते हैं, पर निजी जीवन में संवाद का अभाव झेलते हैं। समाज ने उपलब्धियों को सराहा, पर भावनात्मक संतुलन को अनदेखा किया। यही असंतुलन अब धीमे-धीमे महामारी का रूप ले चुका है।
शहरों की बनावट भी इस अकेलेपन को गहरा करती है। गेटेड सोसायटी सुरक्षा तो देती हैं, पर ऊँची दीवारें संवाद के रास्ते बंद कर देती हैं। पड़ोसी वर्षों तक एक-दूसरे का नाम तक नहीं जानते। पार्कों में लोग साथ-साथ चलते हैं, पर अपनी-अपनी दुनिया में गुम रहते हैं। सार्वजनिक स्थल सिमट रहे हैं, और निजी स्क्रीन फैलती जा रही हैं। बच्चे मैदानों से ज्यादा मोबाइल पर समय बिताते हैं। बुजुर्ग अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे झाँकते हैं, पर बातचीत का अवसर दुर्लभ है। भौतिक विकास ने सुविधाएँ बढ़ाईं, पर मानवीय स्पर्श घटा दिया। यही स्पर्शहीनता दिलों को भीतर से बंजर बना रही है।
फिर भी इस अँधेरे में आशा की लौ टिमटिमा रही है। कई शहरों में सामुदायिक पहलें जन्म ले रही हैं, जहाँ लोग पुस्तक क्लबों, कला कार्यशालाओं और सामाजिक समूहों के जरिये फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर संवाद शुरू हुआ है। नई पीढ़ी अपनी भावनाएँ व्यक्त करने में पहले से अधिक निर्भीक दिखती है। कार्यस्थलों पर वेलनेस कार्यक्रम और लचीले समय की अवधारणा भी जगह बना रही है। यह संकेत है कि समाज समस्या को पहचानने लगा है। और पहचान ही समाधान की पहली सीढ़ी होती है। जब हम स्वीकारते हैं कि अकेलापन सच है, तभी उससे लड़ने की दिशा में ठोस कदम उठते हैं।
अंततः प्रश्न यह नहीं कि शहरों में कितने लोग बसते हैं, बल्कि यह कि कितने दिल सचमुच जुड़े हैं। 1.4 अरब की आबादी में भी यदि व्यक्ति खुद को अनसुना पाए, तो कमी संख्या में नहीं, संवेदना में है। हमें संवाद की संस्कृति को फिर से सांस देनी होगी। रिश्तों में वही निवेश करना होगा, जो हम करियर में करते हैं। पड़ोसी से परिचय, मित्र से बेझिझक बात, परिवार के साथ बिताया समय—ये छोटे कदम बड़े बदलाव की नींव बन सकते हैं। शहर तब सचमुच जीवंत होंगे, जब उनमें रहने वाले लोग एक-दूसरे की धड़कन सुन सकेंगे। भीड़ के बीच भी अपनापन संभव है—बस हमें ठहरकर किसी का हाथ थामने का साहस जुटाना होगा।







.jpg)





34.jpg)










27.jpg)

33.jpg)
2.jpg)





31.jpg)















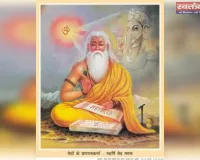



Comments