राजनीति
भारत
राष्ट्रवाद का समावेषी चरित्र,चेतना, लोकतांत्रिक अधिनायकवाद के परहेज की आवश्यकता
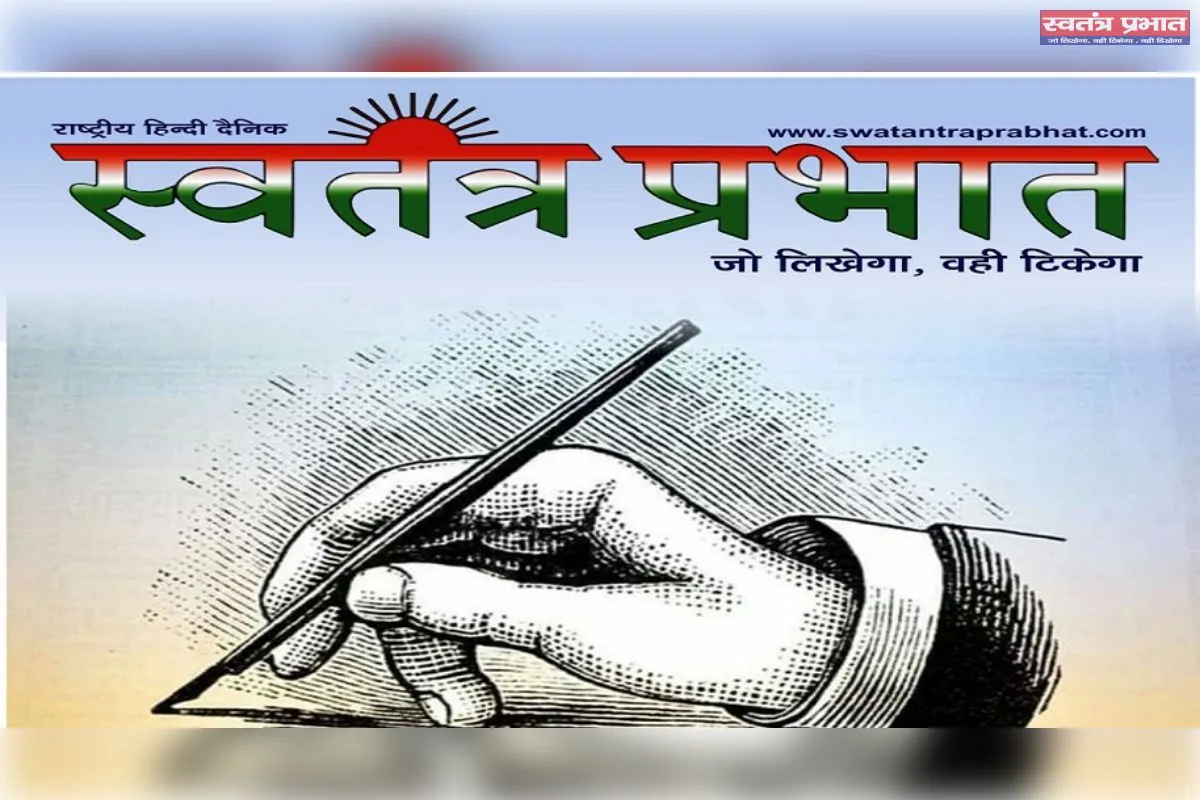
राष्ट्रवाद का मूल चरित्र सार्वभौमिक और समावेशी होता है
राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्र-राज्य की वैचारिक आधारशिला है। यह केवल भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक सत्ता से संबद्ध अवधारणा नहीं है, बल्कि साझा इतिहास, सांस्कृतिक स्मृति, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक उत्तरदायित्वों का समन्वित स्वरूप है। राष्ट्रवाद का मूल चरित्र सार्वभौमिक और समावेशी होता है, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और मानवीय गरिमा जैसे मूल सिद्धांतों को पुष्ट करता है। ऐतिहासिक रूप से यह सिद्ध हुआ है कि राष्ट्र-निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में राष्ट्रवादी चेतना की भूमिका निर्णायक रही है। किंतु जब यही चेतना सत्ता-केंद्रित राजनीति, संकीर्ण वैचारिक आग्रहों और तात्कालिक राजनीतिक लाभों से संचालित होने लगती है, तब यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है।
लोकतंत्र का मूल सिद्धांत सत्ता का निरंतर आवर्तन है। सत्ता का परिवर्तनशील होना शासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाता है। इसके विपरीत, जब सत्ता लंबे समय तक एक ही राजनीतिक शक्ति के अधीन रहती है, तो अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का उदय स्वाभाविक हो जाता है। अवसरवादी राजनीति, पद-लोलुपता और जातिगत समीकरणों का अतिवादी प्रयोग लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ देता है। इस प्रक्रिया में जनता को दूरगामी राष्ट्रीय हितों के स्थान पर तात्कालिक लाभों के प्रलोभन में उलझाया जाता है, जिससे नीति-निर्माण की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास की क्षमता दोनों प्रभावित होती हैं।
लोकतंत्र में राजनीति का उद्देश्य जनभावनाओं का शोषण नहीं, बल्कि उनका संरक्षण और संवर्द्धन होना चाहिए। किंतु जब राजनीति का केंद्र बिंदु सत्ता-प्राप्ति और सत्ता स्थायित्व बन जाता है, तब सिद्धांतों की प्रतिबद्धता कमजोर पड़ जाती है। अवतारवाद, सस्ती लोकप्रियता और भावनात्मक ध्रुवीकरण लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देते हैं। भारतीय राजनीतिक परंपरा में ‘शाम, दाम, दंड, भेद’ को शासन के उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में इनका अति प्रयोग अनुशासन, नैतिकता और संस्थागत विश्वास को क्षीण करता है।
लोकप्रियता को मापने के सुदृढ़ लोकतांत्रिक उपकरणों के अभाव में कई बार संगठित किंतु संख्यात्मक रूप से छोटे समूह नीति-निर्माण पर विपरीत प्रभाव डालने लगते हैं। यह स्थिति बहुमत के शासन के लोकतांत्रिक आदर्श के विपरीत है। दलबदल, अवसरवादी गठबंधन और सिद्धांतहीन राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के प्रमुख कारण बन चुके हैं। भारतीय संविधान के भीतर विद्यमान कुछ प्रक्रियात्मक छिद्रों का उपयोग कर राजनीतिक दल सत्ता-संरक्षण के जटिल ताने-बाने बुनते हैं, जिनके दीर्घकालिक दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र दोनों को भुगतने पड़ते हैं।
जातिवादी राजनीति और लोकप्रियता की व्यावहारिक मजबूरियों ने खाप पंचायतों जैसी समानांतर संरचनाओं को जन्म दिया है। ये संरचनाएँ पंचायती राज व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती हैं, जिससे लोकतंत्र की जमीनी संस्थाएँ कमजोर होती हैं। इसी प्रकार, धर्म और धार्मिक प्रथाओं में समानता तथा स्वतंत्रता का हनन तुष्टीकरण-आधारित राजनीति का प्रतिफल है। लोकतांत्रिक समाज में समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत किसी भी नीति-निर्णय के मूल में होने चाहिए। एकतरफा और भावनात्मक निर्णय इन मूल्यों के प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
अतिराष्ट्रवाद की अवधारणा, जब लोकतांत्रिक विवेक से विमुख हो जाती है, तब तानाशाही प्रवृत्तियों को वैधता प्रदान करने लगती है। सैनिक राष्ट्रवाद, भय की राजनीति और सस्ती लोकप्रियता ने बीसवीं शताब्दी में अनेक देशों में लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त किया है। पाकिस्तान, म्यांमार और उत्तर कोरिया जैसे उदाहरण दर्शाते हैं कि सुरक्षा और राष्ट्रहित के नाम पर सैन्य या अधिनायकवादी नियंत्रण किस प्रकार लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। ये उदाहरण लोकतंत्र के लिए सतत चेतावनी के रूप में देखे जाने चाहिए।
लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य जनता का विश्वास अर्जित करना, उनकी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। किंतु जब शासन सत्ताचरित्र, अवसरवाद और सत्ता में बने रहने की रणनीतियों में उलझ जाता है, तब लोकतंत्र के संस्थागत स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया कमजोर होने लगते हैं। ऐसे समय में समाज के प्रबुद्ध, सजग और जिम्मेदार वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि समय रहते विवेकपूर्ण हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो लोकतंत्र के दुरुपयोग के परिणाम दीर्घकालिक और विध्वंसकारी हो सकते हैं।
अतः यह आवश्यक है कि तात्कालिक लोकप्रियता और अवसरवादी लाभों के स्थान पर संतुलित, समावेशी और बहुआयामी लोकतांत्रिक विकास को प्राथमिकता दी जाए। सरकार, राजनीतिक दल, मीडिया, सिविल सोसाइटी और नागरिक समाज—सभी को मिलकर संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सामाजिक संतुलन की रक्षा करनी होगी। यही समेकित प्रयास राष्ट्रवाद को उसकी मूल, मानवीय और उदात्त चेतना में पुनर्स्थापित कर सकता है तथा लोकतंत्र को अधिनायकवाद की संभावित खतरों से सुरक्षित रख सकता है।
संजीव ठाकुर



7.jpg)
.jpg)













.jpg)
6.jpg)
.jpg)




.jpg)


.jpg)



.jpg)
.jpg)






Comments